गांधी जयंती पर विशेष : 2 अक्तूबर पर दो टूक : सत्याग्रह बनाम सत्ताग्रह
निवेदन : यह प्रस्तुति हमारी है भी और नहीं भी। ‘है’ से ज्यादा ‘नहीं है’ कहना उचित होगा। क्योंकि वस्तुतः इस प्रस्तुति का अधिकांश ‘कथ्य’ और ‘कथन’ शब्दशः एक पुराने आलेख पर आधारित है। पुरानी पीढ़ी के पाठक उस आलेख के बारे आज भी यह कहते हैं कि वह ‘आलेख’ नहीं, ‘आईना’ है। ऐसा आईना, जिसमें सिर्फ बीते ‘कल’ का नहीं, बल्कि ‘आज’ और आने वाले ‘कल’ का ‘चेहरा’ पहचाना जा सकता है। करीब पचास-पचपन साल पूर्व ‘धर्मयुग’ (हिन्दी साप्ताहिक) के विख्यात संपादक धर्मवीर भारती ने यह आलेख (पुस्तक ‘पश्यंती’ में प्रकाशित) लिखा था – ‘चीनी आक्रमण के तुरंत पूर्व का भारत : बौद्धिक चेतना का एक सर्वेक्षण’। उन्होंने इसमें आजादी के बाद ‘गांधीयुग’ के अवसान और नये युग की आहट को आजादी के पूर्व की राजनीति और बाद की राजनीति में आये फर्क के जरिये रेखांकित किया। उन्होंने अपने आलेख में युग बदलने की अपनी ‘समझ’ को स्पष्ट करने के लिए हुए दो शब्दों का प्रयोग किया – ‘सत्याग्रही राजनीति’ और ‘सत्ताग्रही राजनीति’। वह लेख किंचित लंबा है। नए जमाने के तेज रफ्तार में दौड़ती-भागती नयी पीढ़ी उसे पूरा ‘पढ़ने’ को प्रेरित हो, इस ख्याल से हमने उस लेख के कुछ-कुछ अंश शब्दशः प्रस्तुत करते हुए बीच-बीच में ‘नेहरू युग’ के बाद से अब तक के ‘समय’ की ओर इशारा करने वाले कुछ ‘शब्द’ और ‘वाक्य’ जोड़े हैं। बस। यह कितना उचित है और कितना अनुचित, कितना सही है और कितना गलत – यह पाठक ही बता सकते हैं।
हमारे अनजाने में ही एक युग खत्म हो गया है। एक दूसरा युग शुरू हो गया है। इस युग को क्या नाम दिया जाए?
इस नये युग की आहट को, घटना-चक्र को समस्त राष्ट्र की दृष्टि से, समूचे इतिहास के संदर्भ में न देखकर हम इसे ‘मोदी’ के सन्दर्भ में देखें-पहचानें। क्योंकि अब कहा जाने लगा है कि “वे ‘अनिवार्य’ हैं और उनके ‘पर्याप्त’ होने का दावा भी शुरू हो गया है। वे हैं – इतिहास की व्याख्या हमारे लिए कर देते हैं, काफी है। हमें उस दिशा में वक्त बरबाद करने की जरूरत नहीं। हम गरीब मध्यवित्त के पुराने संस्कारों में जकड़े हुए लोग क्या जानें कि तवारीख कैसे बदल रही है। दुनिया में कितनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। चुनाचे जरूरी है कि हम उनकी बातें (मन की बात!) सुनें और उस पर यकीन लाते रहें।”
बौद्धिक निष्क्रियता और धर्म-जैसे अन्धविश्वास का यह युग एकदम पूरी तरह न अवतरित हो पाया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति हावी होने लगी है कि जो कुछ जैसा स्थापित है उसे उसकी सारी असंगतियों, विषमताओं और खोखले समझौतों के साथ ज्यों का त्यों आप स्वीकार कर लें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जरा भी बौद्धिक सक्रियता दिखायी, चिंतन की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तो समझ लीजिए कि कहर बरपा हो गया (यह खतरा तो तलवार की तरह लटक भी चुका है कि ‘देशभक्ति’ और ‘राज-भक्ति’ शब्दों को एक-दूसरे के पूरक और पर्याय सिद्ध किये जा रहे हैं! कोई इस पर असहमति जताने की जुर्रत करेगा, तो उसकी खैर नहीं!)
आजादी के दो दशक बाद से (नेहरू के अवसान के बाद से) हमारे देश के बौद्धिक वातावरण में जो विचित्र प्रकार की निष्क्रियता, बंधाव, गतानुगतिकता, पिटी हुई लकीर पर चलने की भावना आयी (और जो मोदी-उदय से अब नयी बुलंदियों को छू रही है), वह उस वातावरण से बिल्कुल भिन्न है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में (जिसे ‘गांधी-युग’ कहा जाता है) हमारे देश के चिन्तनात्मक और बौद्धिक क्षेत्र में था। उस वक्त इतिहास की एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी और हर आदमी समूचे देश का प्रतीक था।
‘गांधी’ ने हमें बारबार यह बताया कि देश सिर्फ जमीन या नक्शे को नहीं कहते, देश का हर जीवित प्राणी मुजस्सम देश है। मगर आजादी के दो दशक बाद से ही जो नया युग संचरण करने लगा था, वह कुछ भिन्न प्रकार का था। तबसे ही लगने लगा था कि देश में सिर्फ एक व्यक्ति है जो देश का प्रतीक है। वह इतिहास को जैसे समझता है, जैसे समझाता है, जैसे सुलझाता है और जैसे उलझाता है, केवल वही मूल्यवान है। पहले भावना थी कि भारत यानी मैं, यानी आप, यानी वह, यानी हम सब भारत-वासी। धीरे-धीरे अवधारणा उभारी गयी – ‘भारत यानी नेहरू’। उसके बाद ‘इंदिरा ईज इंडिया’ और अब ‘मोदी ईज इंडिया’!

‘राजनीति’ की बात अलग, लेकिन किसी देश की बौद्धिक सक्रियता, जागरूकता और मौलिक चिन्तना शक्ति के लिए इतिहास का इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण और कोई नहीं हो सकता कि देश एक व्यक्ति के समक्ष छोटा या मूल्यहीन साबित किया जाने लगे ; समूचे जन-मानस की संकल्पशक्ति और जीवन-दृष्टि को अक्षम और निःसार बनाने के लिए इससे ज्यादा कारगर और कोई तरीका इतिहास में नहीं रहा है कि एक व्यक्ति की छाया से सारे आकाश को ढंक दिया जाए।लेकिन आजादी के पहले और आजादी के इन दोनों ‘युगों’ का यह फर्क व्यक्तियों का शायद उतना न हो, जितना दो भिन्न जीवन-दृष्टियों का था। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम सारे विश्लेषण को किसी के व्यक्तित्व पर कोई फैसला न बताएं, बल्कि यह देखने की कोशिश करें कि किस युग में किस जीवन-दृष्टि की प्रधानता रही और उसका क्या फल सामने आया।
आजादी की लड़ाई के अंतिम 30 सालों में जो गांधी नेतृत्व करने वाले इतिहास-पुरुषों की कतार में सबसे आगे नजर आते थे उनकी जीवन-दृष्टि क्या थी? इतिहास के दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक़ गांधी को ‘वैष्णवता’ का एक उत्तराधिकार मिला था। उसे उन्होंने जैन-बौद्ध और ईसाई धर्म-चिंतनों के श्रेष्ठतम जीवन-मूल्यों के संस्कारों से समन्वित किया था। उस दृष्टि को उन्होंने राजनीति में प्रतिष्ठित किया। इस तरह उन्होंने राजनीति को ही एक नयी ‘सार्थकता’ दी।उनके पहले राजनीति सत्ता हस्तगत करने और उसे सुरक्षित रखने का कौशल मात्र थी – उसका जीवन के ‘शाश्वत’ नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं था। गांधी ने राजनीति को ‘नैतिक’ मूल्यों से विच्छिन्न नहीं किया वरन् उसे बिना शर्त उनके अधीन रखा। मरण स्वीकार है, सारा देश मिट जाए, लेकिन हमारी निष्ठा की आन न जाने पावे – राजनीति बिना इस मूल्य बोध के आत्मा का हनन कर डालती है। वह माया-जाल बनकर मनुष्य को उलझा देती है।
गांधी की उस जीवन-दृष्टि में राजनीति न तो देश के यथार्थ से कटे हुए बुद्धिजीवियों का चिन्तन-विलास थी, न सत्ता हस्तगत कर उसे सुरक्षित रखने के प्रयास में संलग्न कूटनीतिज्ञों की कुटिलता थी। उनकी जीवन-दृष्टि में राजनीति एक मूल्यपरक साधना थी – इतिहास के संदर्भ में अपना दायित्व निभाते हुए कर्म के माध्यम से आत्मसाक्षात्कार और ‘स्व’ तथा ‘सर्व’ के एकात्म की प्रक्रिया थी। इसीलिए राजनीति की उस धारणा में ईमानदारी, सच्चाई और मूल्य-बोध का बहुत बड़ा स्थान था। आप बड़ा से बड़ा त्याग करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते। वह आप की आत्मा की पुकार है। आप उसे न सुनें तो नुकसान आपका है। आप बड़ी से बड़ी गलती भी कर जाएं तो उसे निहायत ईमानदारी से स्वीकार करने में आपका कुछ नहीं जाता। मिथ्या पथ पर गलती से आप बढ़ गए, आपने गलती महसूस की, सही रास्ते पर आ गए। गलती करना और उसे मुक्तकंठ से स्वीकार कर लेना आत्म-पथ के एक पथिक को आन्तरिक दृष्टि से और भी सम्पन्न बना जाता है। वह अनुभव समृद्ध हो जाता है।
लेकिन जहां राजनीति सत्ता को हस्तगत करने और फिर उसे किसी भी साधन से किसी भी मूल्य पर सहेज कर समेटे रखने की प्रक्रिया बन जाती है, वहां यह स्थिति रहनी संभव नहीं। गलती तो होती ही है। आखिर बड़े-से-बड़ा नेता भी साधारण हाड़-मांस का मनुष्य है। लेकिन ‘सत्तान्वेषी’ और ‘सत्ताग्रही’ राजनीति में अपनी गलती स्वीकार करने में भय लगने लगता है। जनता को प्रभावित करने के लिए राजपुरुष के चारों ओर जो प्रभामंडल बुना गया है वह कहीं धुंधला न पड़ जाए। प्रतिपक्षी कहीं आलोचना का कोई मौका न पा लें। सो नतीजा यह होता है कि एक दूसरी पद्धति विकसित होने लगती है – गलतियां स्वीकारो ही नहीं।
++
गांधी युग में एक शब्द प्रचलित हुआ – ‘सत्याग्रह’। उस शब्द ने देश के एक-एक व्यक्ति में एक निष्ठा जगाई। उसे इतिहास की एक जागरूक, दायित्वयुक्त इकाई के रूप में सार्थकता प्रदान की। उस शब्द की गरिमा थी जो संकल्पयुक्त आचारण से समर्थित थी – ऐसा आचारण जो गलत और सिद्धांतहीन समझौते करने के लिए तैयार नहीं था। साधन और साध्य के मामले में, सत्य के मामले में और अन्य कितनी ही दिशाओं में उस जीवन-दृष्टि के प्रवर्तक ने जो सही समझा उससे तिल भर हटा नहीं और जब जिसे गलत समझा उसे तृण की भांति त्याग देने में रत्तीभर संकोच नहीं किया।
गांधी ने ‘सत्याग्रह’ को अपना सबसे बड़ा ‘शस्त्र’ बनाया। अपने कर्म और क्रिया – अपने व्यवहार और आचरण से इस ‘शस्त्र’ की सीमा-संभावना को उकेरने वाले ‘शास्त्र’ को सूत्रबद्ध किया। उसके कई सूत्र उनके ‘युग’ में प्रकट हुए। जैसे ‘सत्याग्रह’ तभी कारगर ‘शस्त्र’ बन सकता है, जबकि वह हर उस व्यक्ति में ‘जीवन’ के प्रति स्वाधीनता, समता और बंधुता की समझ पैदा करे, जिसे परिवर्तन की जरूरत है। यह समझ ‘सत्याग्रह’ के ‘शास्त्र’ की खोज करने और उस पर अमल करने का ‘हौसला’ पैदा करेगी, तभी सत्याग्रह ‘शस्त्र’ का इस्तेमाल सफल हो सकता है। सत्य के आग्रह से जुड़ा हर ‘संघर्ष’ अहिंसा के जरिये ही सफलता की ओर बढ़ सकता है। अहिंसा के जरिये शत्रु को मारने की ‘युद्धनीति’ पर ही पहला प्रहार होता है। किसी भी संघर्ष में कोई बाहरी ‘हथियार’ किसी व्यक्ति के अंदर के ‘भय’ को पैदा होने से रोक नहीं सकता।
‘सत्याग्रह’ शब्द को गांधी की जीवन-दृष्टि, आचरण पद्धति और मूल्य समन्वित राजनीति ने नैतिक साहस और आचरण का सम्बल प्रदान किया। वहां सब कुछ मिट जाए, मगर सिद्धांत है वह है। उस मामले में समझौता नहीं होगा। सिद्धांतों को नष्ट कर कोई भी समझौता करना अपनी आत्मा को नष्ट करना है। इसलिए किसी भी युग के बदलने को समझने का सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, जीवन-दृष्टि का होता है, जो समग्र देश के मानस को प्रभावित करने लगती है।
‘सत्याग्रही राजनीति’ में सत्य पर आग्रह रखनेवाला चिन्तन और जीवन-दृष्टि बेलौस ईमानदारी की मांग करते हैं। और ‘सत्ताग्रही राजनीति’ में? ‘सत्ताग्रह’ का तरीका – उसका चिन्तन और जीवन-दृष्टि – नितांत अलग होता है। बाहर से खूबसूरत चेहरे, मुखौटे और ज्योतिमंडल जितने बढ़ते-जाते हैं अंदर से कहीं कुछ उतना ही खोखला, सामर्थ्यहीन, संकल्पहीन, निष्फल और शून्य होता जाता है। आतंरिक असंगतियों की उलझन में अन्दर से मूल्यान्वेषण, आत्म-विश्लेषण और सच्चाई को जानने और खोजने की आकुलता लगभग समाप्त सी हो जाती है। अन्दर अन्तरात्मा की उस बंद हुई आवाज को भुलाने के लिए हम बाहर बोलना शुरू करते हैं और फिर इस कदर बोलने लगते हैं कि बोलते ही जाते हैं। यहां तक कि हमें यह भी खबर नहीं रहती कि हम क्या बोल रहे हैं और सप्ताह-पंद्रह दिन बाद हमें पहले बोले हुए वक्तव्यों का खंडन और निराकरण करना पड़ता है।
बदलते समय की यह पहचान है कि यही वह समय होता है जब चिन्तन गौण हो जाता है, चंद नारे दर्शन और विचारों का स्थान लेने लगते हैं (सत्याग्रह के संघर्ष के दौर में भी ऐसा होने का खतरा था)। यही वह समय होता है जब चंद खूबसूरत शब्दों से अंदर का खोखलापन ढांकने की कोशिश होने लगती है (सत्याग्रही इसके प्रति गाफिल नहीं रह सकता।)। यही वह समय होता है, जब शब्दों के पीछे आचरण, निष्ठा, चिन्तन, गंभीर अर्थ नहीं रह जाते। तब उन्हें एक बाहरी चमक-दमक प्रदान की जाती है। उन्हें प्रचार-पत्रों में छापकर, प्रसार-यंत्रों से प्रसारित कर गुंजाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अक्षम और आधारहीन होने के कारण वे बार-बार लड़खड़ाकर गिरते नजर आते हैं। (सत्याग्रही अपनी पिछली बात – पिछले वक्तव्य – का खंडन नहीं करता। वह तो बाद के वक्तव्य या बात को उससे ज्यादा बेहतर और कारगर कहता है।
एक ऐसी स्थिति (भी) पैदा हो जाती है कि जहां एक ही शब्द की परिधि में दो बिल्कुल उलटे अर्थ एक साथ प्रतिष्ठित होने की कोशिश करने लगते हैं। किसी दूसरी स्थिति में जहां इस अन्तर्विरोध पर लोग चौकते, वहां ऐसे युग में यह सब परिचित-परिचित-सा लगने लगता है। चारों ओर हम पाते हैं कि एक असंगतिपूर्ण स्थिति है – खास तौर से मूल्यों और सिद्धांतों की दुनिया में, जहां दो नितांत विरोधी बातें एक ही सैद्धांतिक उद्घोष में साथ-साथ प्रतिष्ठित नजर आती हैं।इसके कई उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि हम नाम लेते हैं प्रजातंत्र का, जम्हूरियत का, साधारण जन का, और करते वह सब हैं जो ‘व्यक्तिपूजा’ को बढ़ावा दे और प्रजातंत्र की उन्मुक्त चेतना को धीरे-धीरे संकुचित और कुंठित बनाता जाए।
यह सब एक अजीब सी अन्तर्विरोध और वैषम्यवाली जीवन-दृष्टि का अवश्यंभावी परिणाम है। यह परिणाम केवल राजनीति में नहीं दृष्टिगोचर होते, उन राजनीतिक केन्द्रों के इर्द-गिर्द पनपनेवाली समस्त साहित्य-चिन्तन और संस्कृति में ये सारे अन्तर्विरोध पनपने लगते हैं। यह विघटन यहीं पर रुकता नहीं। यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। धीरे-धीरे संस्कृति की मूल जाग्रत् चिन्तन-प्रक्रिया समाप्त होने लगती है। मानस में एक संवेदनहीन जड़ता धीरे-धीरे पैठने लगती है। जो भी हो सब ठीक है। बस, जितना जो बना हुआ है उतना बना रहे। अगर अंदर से टूटता भी जाए तो कम से कम ऊपर से यह आभास रहे कि हमने कुछ खोया नहीं। ऐसी जड़ स्थिति में अगर अस्वस्थ असंगत विचार हम पर आक्रमण करें तो हममें प्रतिरोध करने की आत्मिक शक्ति नहीं रह जाती। अगर हमारा बहुत कुछ मूल्यवान छिन गया है जो हमारी समृद्ध विचार-परम्परा का एक महत्वपूर्ण अंश था, तो हम यह कहकर संतोष दे लेते हैं कि वह कुछ खास नहीं था। चला गया तो जाने दो।
जब जीवन-दृष्टि उलझी हुई हो और मूल्यबोध धुंधला हो, तब हमारी मनोभूमि जरूर बंजर, पथरीली और बियावान होने लगती है। बाहर के क्रिया-कलाप, कथन और आचरण तो उसे प्रतिबिम्बित मात्र करते हैं।
++
इतिहास गवाह है कि जनता से कभी-कभी गांधी की भी ठनी। गांधी ने जब कभी अपने को पृथक महसूस किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे सत्य की ओर रहेंगे। अगर वे नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें सत्य नहीं दीख रहा है, वे चिन्तन करेंगे, आत्मशुद्धि करेंगे। लेकिन जब तक वे उसे सत्य नहीं मान लेते तब तक वे कोई भी पथ नहीं अपनाएंगे, चाहे इससे लोकप्रियता घटे या बढ़े। इसीलिए जनता से गांधी की पृथकता और अन्तरंग एकसूत्रता दोनों ही सत्य के परिप्रेक्ष्य में, सत्य के आग्रह के लिए थीं।इसलिए वे अपनी बड़ी से बड़ी भूलों को स्वीकार करने में पल भर हिचकिचाते नहीं थे। उनकी मूल स्वीकृति भी उनके आन्तरिक विकास की एक नयी, आगे ले जानेवाली, कड़ी बन जाती थी।गांधी की टेक थी कि जब तक मैं न जान लूं कि यह सच है, मैं इस रास्ते को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यह गांधी के आत्मविश्वास का प्रमाण था, लाचारी नहीं। क्या आज के रहबरों का नेतृत्व वही आत्मविश्वास है? या कि वह आत्मविश्वास की कमी या लाचारी का द्योतक?
आज जो ‘नायक’ नेतृत्व की अगली कतार में हैं, उन्होंने जो जीवन-दृष्टि अपनाई – उस जीवन-दृष्टि ने जो रास्ता अपनाया, क्या वह भी ‘सत्याग्रह-मार्ग’ है? क्या जोर-जोर से उद्घोषित पहले वाली नीतियां, इतिहास की पिछली व्याख्याएं, जो बदली गयीं, वे सत्य के आग्रह के लिए हैं? या इसलिए जनता ने इस समय अपना ‘रास्ता’ (अस्पष्ट, बेपहचान!) निर्धारित कर लिया और रहबरे कारवां दौड़कर कारवां के आगे हो जाने की होड़ में है कि नहीं तो वे पीछे के रेगिस्तान में अकेले छूट जाएंगे? पहले एक रास्ते के लिए जिद ठानना और फिर दौड़कर दूसरे रास्ते की रहबरी स्वीकार कर लेना – इन दोनों के बीच क्या वही आत्मिक विकास और मानसिक प्रौढ़ता की प्रक्रिया है जो गांधी की जीवन-दृष्टि में थी? या एक भय है कि कहीं हमसे यह बागडोर छूट न जाए?

आज की जवान और नयी पीढ़ी की नाराजगी और निराशा, बेचैनी और उत्तेजना में निहित नकारात्मकता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आम जन की असहाय ‘याचक’ जैसी छवि में निहित स्पष्ट सवाल तो यह है कि आजादी के बाद से आज तक देश में ‘गांधी’ के नाम पर, ‘सत्याग्रह’ को किस रूप में स्वीकार किया गया और किया जा रहा है? प्रेरणा के रूप में या मजबूरी के रूप में? मुखौटा के रूप में या मोहरा के रूप में?
आज 21वीं सदी में ‘भारत’ का लोकतंत्र ‘विकास’ के जिस पथ पर चल रहा है, उसमें क्या इस दुर्भाग्य से मुक्ति की उम्मीद की रोशनी है? याकि आजादी के दो दशक बाद से इतिहास के घटना-चक्र के संदर्भ में जो कुछ ‘सवाल’ के रूप में प्रस्तुत था, वह अब ‘समस्या’ नहीं बल्कि ‘संकट’ बनकर पसर गया है? आज के नायकतत्व में ठोस बौद्धिक आधार के, संकल्प के और इतिहास-दृष्टि के अभाव का क्या यह संकेत नहीं कि आज के स्वयंभू नायक पहले जिसे इतिहास की अपनी व्याख्या मानते हैं, उसे न केवल एकमात्र प्रामाणिक मानने का दम्भ प्रकट करते हैं, बल्कि अगर कोई भी उसमें संशोधन पेश करे तो वे इस कदर खीझ उठते हैं, इस कदर झुंझला उठते हैं कि आपे से बाहर हो जाते हैं? यह उनकी विचित्र सी क्षणिक या तात्कालिक उत्तेजना या प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह उनके ‘चरित्र’ का स्थायी भाव है, आदत है – क्या यह कहना गलत या अत्युक्ति है?
++
हमारे युग के नायकों की दृष्टि और कार्य-व्यापार से अक्सर यह झलकता है कि उन्होंने पिछड़े देश-समाज के लिए, 21वीं सदी में भी 19वीं-20वीं सदी में रहनेवाले ‘लोक’ के लिए, जेट विमानों पर चक्कर लगाकर देश-विदेश से जो ज्ञान बटोरा है, उसकी अवहेलना की जा रही है। वे आगे हैं और जनता पिछड़ रही है, उनके पीछे चलने को तैयार भी नहीं है। लेकिन अचानक किसी मोड़ पर ये नायक पाते हैं कि इतिहास उन्हें गलत साबित करता है, लोक उनके अनुमानित किये गए घोषित पथ से बिल्कुल पृथक एक दूसरी दिशा अपनाता है। ये पाते हैं कि पुराने युग में रहने वाला सामान्य जन इनसे ज्यादा साफ दृष्टि से इतिहास को देख रहा है और वह उठकर खड़ा हो गया है, अपनी नियति के सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए सन्न्नद्ध! तब कथित ‘नायकों’ और कथित इतिहास-द्रष्टाओं की बड़ी विचित्र हालत हो जाती है। एक आकस्मिक विपर्यय उनके लिए अनिवार्यता बन जाता है।
इस स्थिति-परिस्थिति का तोड़ या समाधान क्या है, इस समझ से शुरू करने के सिवा कि वास्तविक संकट मूल्यों का है, जीवन-दृष्टि का है? हर ‘नायक’ जनता के प्रति अपनी‘समझ’ को टटोले, उसमें सुधार करे, उसमें परिवर्तन लाये तो सामान्य जन की जागृत चेतना उनके लिए एक नये उत्साह, गहन निष्ठा, निर्भीक साहस और स्पष्ट विवेचन की भूमिका बन सकती है। तब वर्तमान स्थिति-परिस्थिति देश के बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। राजनेता राजनीति की दृष्टि से, अर्थशास्त्री आर्थिक दिशाओं को विभिन्न और दृष्टिकोण से बौद्धिक जमातें एवं साहित्कार-इतिहासकार सामान्य जन के साथ जीवन-दृष्टि का सम्यक आकलन करें – समाधान का रास्ता यहां से शुरू होता है, इसकी पहचान किये बिना, इसको साधे बिना – क्या कोई ऐसा बदलाव संभव है, जिसको पूरा देश-समाज ‘विकास’ का पर्याय माने?
हेमंत
++++


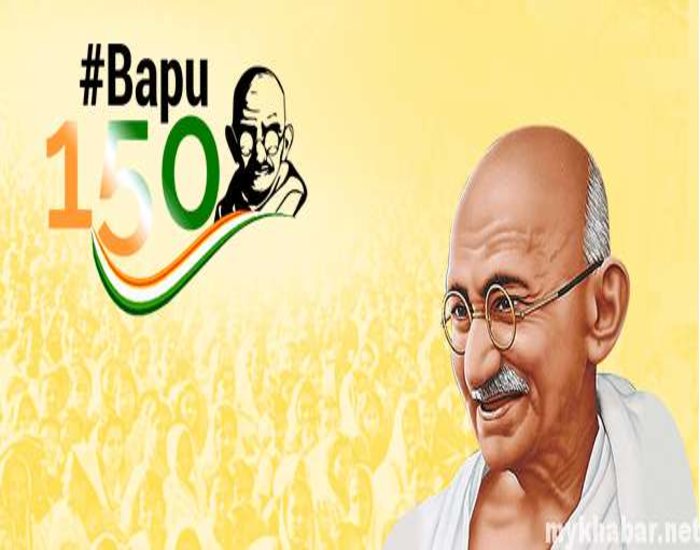
Comments are closed.