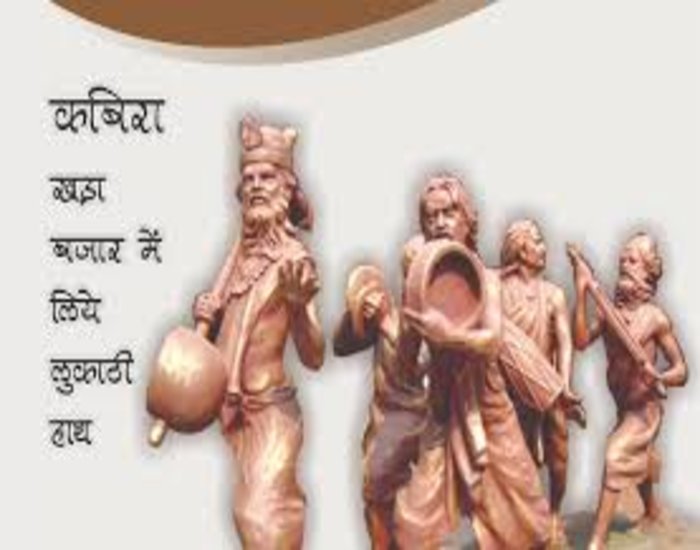जब कभी ‘संस्कृति’ के सवाल पर बात होती है, अक्सर हम एक सांस में बोलने लगते हैं। सबकी मान्यताएं अलग और स्तर अलग। अक्सर यह भी होता है कि हम संवाद के लिए एकजुट होते हैं लेकिन सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। हमारी सोच और दृष्टि पर मान्यता और स्तर की ऐसी धूल जमी रहती है कि हम मिल-बैठ कर भी उसको साफ नहीं कर पाते। संवाद हो, तो सफाई हो। संवाद ही नहीं हो पाता। होता भी है तो वह बहरों का संवाद जैसा दिखता है। इसकी कोई एक वजह नहीं होगी। फिर भी मेरे मन में यह सवाल उठता है, आप के मन में भी उठता होगा कि क्या इसकी कोई खास वजह है?
मैं खुद को भारत के करोड़ों अनपढ़, बेजुबान और मौन लोगों की कतार में खड़ा कर इस सवाल के बारे में सोचता हूं, तो एक खास जवाब मिलता है। वह है – हीनताबोध! कि हम गुलाम थे। कि चंद सैकड़ा लोग हम पर ढाई सौ साल राज कर गये। कि हम कमजोर थे, इसलिए उन्होंने हमें – भारत को – अपने अधीन किया। कि वे हमें लूट गये। इसके खिलाफ हम लड़े और आजाद भी हुए, लेकिन इस क्रम में हम स्वाधीन से ‘आत्महीन’ हुए। क्या हमारा अपनी संस्कृति के बारे में बहरों की तरह संवाद करना उसी आत्महीनता की सहज मानवीय प्रतिक्रिया है?
मुझे लगता है कि हां, यह एक खास वजह हो सकती है। हालांकि जब कभी मैं भारत के पढ़े-लिखे, बौद्धिकों और मुखर लोगों की जमातों में बैठकर सोचता हूं, तो मुझे हीनताबोध का दूसरा सिरा भी नजर आता है। उन जमातों में होने वाली मुखर बहस इस ‘गर्वबोध’ को रेखांकित करती है कि यहां जो था, वह सब अच्छा था! कि कोई हमें लूटने आया, इसका मायने ही है कि हम सम्पन्न थे। यह मुझे पेंडुलम की तरह डोलते ‘हीनताबोध’ के दूसरे सिरे की अभिव्यक्ति लगती है। मैं नहीं जानता कि इसमें कौन कितना सही है।
मैं फिलहाल सही-गलत का सवाल उठा भी नहीं रहा। मैं यह रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि संस्कृति से जुड़ा हर सवाल ‘स्व’ को परिभाषित करने, व्याख्यायित करने से शुरू होता है और आजकल ‘स्व’ की नयी परिभाषाएं गढ़ने की कोशिशें चल रही हैं। वैश्वीकरण और विश्व बैंक के संदर्भ में आज देश में संस्कृति को परखने के क्रम में स्व की नयी तलाश की यह कोशिश कुछ ज्यादा स्पष्ट, तेज और आक्रामक नजर आती है। इस सिलिसिले में ‘भारतीयता’ यानी ‘भारतीय संस्कृति’ की पहचान करने के बहाने हिंदुत्व के स्व की परिभाषित करने का प्रयास नयी बुलंदियों पर है ही। 6 दिसम्बर, 1992 के बाद से मुस्लिम ‘स्व’ की भी नयी परिभाषाएं हो रही हैं। अगर विषयांतर न माना जाये तो यहीं इतना कहना उचित होगा कि जिनको हम परम्परा से ‘इहलोकवादी’ कहते हैं, उनके चिंतन में कुछ निराशा दिखती है। वे पहले कहते थे कि सार्वजनिक जीवन में धर्म संबंधी मामलों को नहीं लाना चाहिए। कि धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ यही है। वे ही अब कहते हैं कि इसमें ‘धर्मनिरपेक्षता’ हार गयी है। दूसरी ओर जो धार्मिक मुसलमान हैं, उनको यह बोध हुआ कि धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक जीवन में वे अच्छे मुसलमान नहीं साबित हुए। उनमें यह सोच मजबूत हुई है कि वे अपनी धार्मिक पहचान को ज्यादा सही व सच्चा बनाने की कोशिशि करें। इसके लिए राजनीति से खुद को अलग करें क्योंकि यह राजनीति अंध सत्तावाद का खेल है। (जारी)